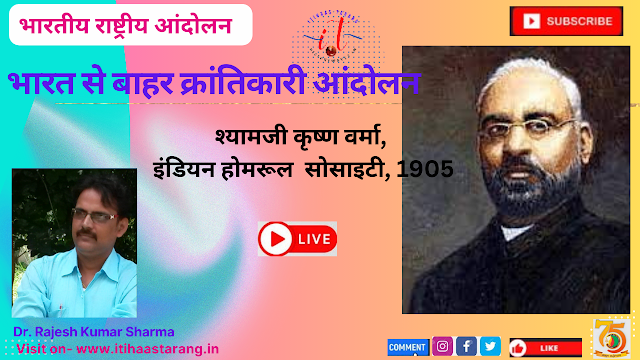विदेशों में क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी आन्दोलन -
भारत के बाहर भी क्रान्तिकारी क्रियाशील हुए। इंग्लैण्ड में श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर ने, फ्रांस में मैडम कामा ने और अमेरिका में लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद के संगठन में अग्रणी भूमिका निभाई। विदेशों में आंदोलन के प्रचार-प्रसार का श्रेय सर्वप्रथम श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से थे। वे तिलक की सिफ़ारिश पर लंदन गए थे और 1904-14 के बड़े ही नाजुक दौर में उन्होंने लंदन, पेरिस और जेनेवा में भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़े ज़ोर-शोर से प्रचार अभियान चलाया था। इस कार्य में उनके सहयोगी थे - भाई परमानंद, मैडम कामा, विनायक दामोदर सावरकर आदि। कुछ अँग्रेज़ मित्रों की सहायता से उन्होंने ’इंडियन सोशियोलोजिस्ट’ नाम से अपनी एक पत्रिका शुरू की ताकि इसके द्वारा भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा जा सके और भारतीयों की शिकायतों को प्रकाश में लाया जा सके। उन्होंने 1905 में होम रूल सोसाइटी तथा इंडिया हाउस की भी स्थापना की। फेलोशिप पर लंदन आने वाले भारतीय विद्यार्थियों को इन संस्थाओं में रहने की सस्ती जगह मिल जाती थी और साथ ही लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए ये ऐसी जगहें हो गई थीं जहाँ वे एक-दूसरे से मिल सकते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन को इंग्लैंड में लोकप्रियता मिली और वह मजबूत हुआ। एक ही साल के अंदर इसकी सदस्य संख्या 119 हो गई। इंग्लैंड में लोकतांत्रिक चेतना तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा गठित राजनैतिक गतिविधियों से अनेक भारतीयों में सोई हुई राष्ट्रीय भावना जाग उठी। आरंभ से ही श्यामजी सक्रिय प्रतिरोध की अमोघ क्षमता के बारे में सहमत थे और वे इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बड़ी प्रबल शक्ति मानते थे। आगे चलकर उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में शक्ति के इस्तेमाल का खुलकर प्रचार किया। उन्होंने यह प्रचारित किया कि भारत में अत्याचारी विदेशी शासन को हिंसक साधनों से ही समाप्त किया जा सकता है और इसका एकमात्र कारगर रास्ता है - रूसी पद्धति।
इस गुट के अन्य महत्त्वपूर्ण सदस्य थे - वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वी0 एस0 अय्यर, तिरुमल आचार्य आदि। जब जी0 एस0 खपरिडे, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, राम भुजदत्त और विपिन चंद्र पाल, इंग्लैंड में आ गए तो लंदन एक सक्रिय केंद्र हो गया। यद्यपि हरदयाल को छोड़कर अन्य किसी ने हिंसा की नीति का समर्थन नहीं किया, फिर भी उनके भाषणों ने यूरोप में रहने वाले भारतीयों में क्रांति की चेतना फूॅंकी। जब जो ब्रिटिश अधिकारी भारत और उसके बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अनुचित तरीक़े अपना रहे थे उन्हें आतंकित करने की नीति अपनाने के लिए इन भारतीय क्रांतिकारियों ने ऐसे अधिकारियों को अपने मार्ग से हटाने का निश्चय किया। उन्होंने लॉर्ड कर्ज़न, लॉर्ड किचनर तथा सर कर्ज़न वायली’ (जो भारतीय मामलों के सेक्रेटरी आफ़ स्टेट के राजनैतिक परिसहायक या ए०डी०सी० थे) की हत्या की योजना बनाई।
विदेशों में इन क्रांतिकारी समूहों की गतिविधियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समर्थन जुटाने और भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य का समर्थन करने और समग्र क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और गठबंधन बनाने की मांग की।
विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ - पृष्ठभूमि
विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ - विशेषताएँ
.20वीं सदी की शुरुआत में विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों की कई विशिष्ट विशेषताएं थीं जिसका उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है -
केन्द्रों एवं समितियों की स्थापना - भारतीय क्रांतिकारियों ने विदेशों में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रों एवं समितियों की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे ’इंडिया हाउस’ के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारतीय छात्रों और बुद्धिजीवियों के लिए एक सभा स्थल के रूप में कार्य किया, भारत के कट्टरपंथी युवाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की, और ’द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट’ प्रकाशित किया। पत्रिका और इन केंद्रों ने क्रांतिकारी चर्चा, योजना और आयोजन के लिए एक मंच प्रदान किया।
क्रांतिकारी साहित्य पर ध्यान - भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विदेश यात्रा करने की प्रमुख प्रेरणाओं में से एक क्रांतिकारी साहित्य को प्रकाशित और प्रसारित करने का अवसर था। ब्रिटिश-नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर रहकर वे प्रेस अधिनियमों को दरकिनार कर सकते थे, जो ब्रिटिश शासन की आलोचना करने वाले प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाते थे। साहित्य के प्रकाशन और वितरण ने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रमुख क्रांतिकारियों को शामिल करना - विदेशों में क्रांतिकारी केंद्रों ने उल्लेखनीय क्रांतिकारियों को सदस्य के रूप में आकर्षित किया। विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल ढींगरा जैसी शख्सियतें लंदन में इंडिया हाउस से जुड़ी थीं। इन व्यक्तियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को आकार देने और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण - ब्रिटिश निगरानी और दमन की तीव्रता के कारण क्रांतिकारियों के लिए लंदन से दूसरे शहरों में स्थानांतरित होना आवश्यक हो गया। लंदन तेजी से खतरनाक होता गया, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियाँ पेरिस, जिनेवा और बर्लिन जैसे अन्य यूरोपीय शहरों में स्थानांतरित हो गईं। इससे क्रांतिकारियों को अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण में अपना काम जारी रखने की अनुमति मिल गई।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध और गठबंधन - विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों ने सक्रिय रूप से विदेशी समाजवादियों, बुद्धिजीवियों और उपनिवेशवाद-विरोधी कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन और संपर्क की मांग की। उन्होंने उन व्यक्तियों और संगठनों के साथ सहयोग किया जिन्होंने स्वतंत्रता और क्रांति के अपने लक्ष्यों को साझा किया। इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग ने वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की।
रणनीतिक उद्देश्यों के लिए निर्वासन का उपयोग - क्रांतिकारियों ने अपने निर्वासन का उपयोग भारत की मुक्ति के लिए संसाधन और समर्थन इकट्ठा करने के लिए किया। उन्होंने विदेशों में सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों और सरकारों से हथियार, धन और राजनीतिक समर्थन मांगा। निर्वासन ने उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाने और समन्वय करने का अवसर भी प्रदान किया।
कुल मिलाकर, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों ने भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित होने, साहित्य प्रकाशित करने, नेटवर्क स्थापित करने और अपने उद्देश्य के लिए सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। इन गतिविधियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को आकार देने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता और समर्थन पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इंडियन होम रूल सोसाइटी (1905)
1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी वास्तव में एक महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्व-शासन या घरेलू शासन की अवधारणा की वकालत करना था। सोसायटी ने भारतीय छात्रों और बुद्धिजीवियों को राष्ट्रवादी विचारों पर चर्चा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया और इसने क्रांतिकारी आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इण्डियन होमरूल सोसायटी के सदस्यों का पहला निशाना बने - कर्ज़न वायली। अमृतसर से आए इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी श्री मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई, 1909 को उन्हें अपनी गोली से मार गिराया। ढींगरा ने अपनी अंतिम इच्छा यह व्यक्त की कि उनके अंतिम संस्कार हिंदू धर्मविधि के अनुसार संपन्न किए जाएँ। किंतु इंडिया हाउस ने उनकी यह छोटी सी माँग भी ठुकरा दी जिससे उसकी ह्रदयहीनता का संकेत मिलता है। 17 अगस्त, 1909 को ढींगरा का दाह-संस्कार कर दिया गया। भारत के कई नेताओं - वी०सी० पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले इत्यादि ने शहीद मदनलाल ढींगरा की कड़े शब्दों में निंदा की, मगर कई अँग्रेज़ राजनीतिज्ञों ने उनकी प्रशंसा की और आयरलैंड के अखबारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा - “मदनलाल ढींगरा को, जिन्होंने अपने देश की ख़ातिर अपना जीवन न्योछावर कर दिया, आयरलैंड अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।“ डब्लयू0 एस0 ब्लण्ट ने अपनी डायरी में लिखा - “लोग इसे राजनैतिक हत्या कहते हैं जब कि ऐसा कहना उनकी ही लक्ष्य-सिद्धि के लिए घातक है, पर यह बकवास है। यह तो बस स्वार्थी शासकों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए चौका देने वाली कार्यवाही थी कि स्वार्थ में भी निर्लज्जता की एक सीमा होती है।
कर्ज़न वायली की हत्या को ब्रिटिश सरकार ने गंभीर रूप में लिया। इंग्लैंड के राजा ने एक पत्र में गवर्नर-जनरल को चेतावनी दी कि वे ऐसे युवकों को उस देश में न आने देने के लिए क़दम उठाएँ क्योंकि ये वहाँ जाकर अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की शिक्षा ही लेते थे।
मगर भारत में सरकारी जुल्म के बावजूद हिंसा की घटनाएँ होती रहीं। भारत और भारत से बाहर जो एक के बाद एक हत्या की घटनाएँ हुईं उनके अधिकारियों को यह प्रमाण मिल गया कि भारत तथा भारत से बाहर की क्रांतिकारी समितियों में घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि संगठित राजनैतिक दलों में से कोई भी इन हत्याओं की कार्यवाही में शामिल नहीं था, फिर भी भारत की ब्रिटिश सरकार इस बात से सहमत थी कि ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के पीछे गहरी साज़िश है। आगे चलकर जब नासिक में जैक्सन की हत्या कर दी गई तो उनका डर पक्का हो गया क्योंकि इस हत्या में लंदन गुट द्वारा भेजी गई बाटनिंग पिस्तौलों में से एक का उपयोग किया गया था। भारत सरकार के आदेश पर दामोदर सावरकर को गिरफ्तार करके भारत भेज दिया गया और नासिक षड्यंत्र मुक़द्दमें में उन्हें सजा हो गई।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडिया हाउस द्वारा स्थापित नेटवर्क भारत में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के प्रयासों को संगठित करने और समन्वय करने में समाज द्वारा प्रदान किए गए संपर्क और समर्थन महत्वपूर्ण थे।
कुल मिलाकर, इंडियन होम रूल सोसाइटी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी आंदोलन था जिसने भारतीय बुद्धिजीवियों, छात्रों और कार्यकर्ताओं को भारत के लिए स्वशासन के विचार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसका प्रभाव लंदन से आगे तक बढ़ा, इसके सदस्यों ने यूरोप, अमेरिका और भारत में अपना राष्ट्रवादी कार्य जारी रखा और भारतीय स्वतंत्रता के लिए व्यापक संघर्ष में योगदान दिया।
सावरकर पर मुक़द्दमा चलने के बाद लंदन गुट ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश-विरोधी गतिविधियाँ ज़ारी रखने के लिए अब लंदन कोई सुरक्षित जगह नहीं है, अतः वे वहाँ से पेरिस या अन्य यूरोपीय राजधानियों में चले गए। इन नेताओं में प्रमुख थे - चट्टोपाध्याय, अय्यर और लाला हरदयाल। इन लोगों ने क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार किया, यूरोपीय महाद्वीप की क्रांतिकारी एजेंसियों से संपर्क स्थापित किए अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजनाएँ बनाई और देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए भारत को हथियारों की सप्लाई की। पेरिस इंडियन सोसायटी से जुड़े हुए प्रमुख भारतीय थे- मैडम भीखाजी कामा, एस0 एस0 राणा, एम0पी0टी0 आचार्य, के0 आर0 कोटवाल आदि। भारत में भी हत्याओं का क्रम जारी रहा। 13 नवम्बर, 1909 को लॉर्ड और लेडी मिंटो की गाड़ी पर अहमदाबाद में बम फेंका गया। इस समय वाइसराय लॉर्ड मिंटो, जो कंज़र्वेटिव पार्टी के थे, और लॉर्ड मार्ले में, जो लिबरल पार्टी के थे, मतभेद हो गए। लॉर्ड मिंटो दमन की नीति अपनाना चाहते थे और मार्शल लॉ लागू करना चाहते थे क्योंकि मिंटो-मार्ले सुधार के बावजूद भारत की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था, मगर लॉर्ड मालें इस पक्ष में नहीं थे। उन्होंने लिखा- “मार्शल लॉ को, जो कि सभी क़ानूनों को निलंबित कर देने का एक बेहतरीन नाम है, लागू कर देने से भारत में हत्या-संगठनों का उससे अधिक सफ़ाया नहीं हो पाएगा जितना कि इसी तरह के संगठनों का इटली, रूस अथवा आयरलैंड में हो सका“।’
सिंगापुर विद्रोह, 1915 -
कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएॅं -
इसी समय, बर्लिन में बसे कुछ भारतीय आंदोलनकारी, जिनका संपर्क अमरीका में ग़दर क्रांतिकारी रामचंद्र से था, जर्मनी की मदद से विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों से संपर्क करने और उन्हें विद्रोह के लिए तैयार करने की कोशिश करने लगे। जर्मनी की सहायता से, 1 दिसम्बर 1915 ई0 को काबुल में भी राजा महेंद्रप्रताप के नेतृत्व में एक अस्थायी और अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई जिसमें प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान केन्द्रीय शक्तियों के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की गई थी। इनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे - मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी० पिल्ले, शमशेर सिंह, डॉ० मथुरा सिंह, खुदाबख़्श और मुहम्मद अली । बरकतुल्ला प्रधानमंत्री चुने गए। इस अंतरिम सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीय आन्दोलन के लिए कट्टर अमीरों के साथ-साथ रूस, चीन और जापान से समर्थन हासिल करना था। इस अंतरिम सरकार को अफगान सरकार से आंतरिक प्रशासन से महत्वपूर्ण समर्थन मिला। हालॉंकि रिच ने खुले समर्थन की घोषणा करने से इन्कार कर दिया। अंतरिम सरकार ने सहायता के लिए कई देशों की सरकारों से संपर्क किया और राजा महेंद्र प्रताप लेनिन से भी मिलने गए। लेकिन इस तरह की तमाम कोशिशों का कोई खास नतीजा नहीं निकला और अन्ततः ब्रिटिश सरकार के दबाव में इसे 1919 में अफगानिस्तान से वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार सशस्त्र विद्रोह के बल पर अँग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य पूरा न हो सका।
इसी तरह हिज्रत आंदोलन भी भारत में शुरू किया गया और कई मुसलमान युवक भारत की सीमा पार कर अफ़गानिस्तान और तुर्किस्तान पहुँचे और वहाँ खुदाई सेना की स्थापना की। इनकी कार्रवाइयों में से एक रेशमी रूमाल षड्यंत्र भी था। रूमाल पर प्लान लिखकर एक नौकर के हाथ भारत भेजा गया मगर नौकर अमृतसर पहुँचने पर घबरा गया और उसने क्रांतिकारी तंत्र से संबंधित व्यक्ति को देने के बजाय रूमाल अपने मालिक को दे दिया। मालिक डिप्टी कमिश्नर का मित्र था और उसने यह रेशमी रूमाल उसके हवाले कर दिया जिससे सरकार को इस षड्यंत्र का पता चल गया और उन्होंने कथित लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। इस प्रकार यह षड्यंत्र भी कामयाब नहीं हुआ।
मूल्यांकन -
इस प्रकार विदेशों में बसे तमाम नवयुवकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा फहराए रखा और अपने साहस और त्याग से अपनी देशभक्ति का सबूत दिया। यद्यपि विदेशों में हुये भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन भी धीरे-धीरे ठंडा पड गया। वास्तव में एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में आन्दोलन की असफलता निश्चित थी। इसने जनता को गतिमान नही बनाया और वास्तव में जनता के साथ इनका भी कोई आधार नही था लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद के विकास में क्रांतिकारियों का बहुमूल्य योगदान रहा। हालॉंकि राजनीतिक रूप से अधिकांश लोग क्रांतिकारियों के राजनीतिक दृष्टिकोण से सहमत न थे फिर भी ये क्रांतिकारी अपनी वीरता के कारण अपने देशवासियों में बेहद लोकप्रिय हुये।
विदेशी धरती पर हुये इन क्रान्तिकारी आंदोलनों का यदि हम सिंहावलोकन करें यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि इनकी तकनीक और तरीक़े एक जैसे थे। इनका यह विश्वास था कि अहिंसा और शांतिमय ढंग से आज़ादी नहीं मिल सकती। ये ब्रिटिश सरकार के अफ़सरों और उनकी सहायता करने वालों के मन में आतंक पैदा करना चाहते थे ताकि वे महसूस करें कि उनका जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं है और वे इस दबाव में आकर देश छोड़कर चले जाएँ। 1913-1918 के दौरान क्रांतिकारियों, विशेषकर गदर पार्टी ने महसूस किया कि सिर्फ़ आतंक से अँग्रेज़ों को नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने एक प्रकार के गुरिल्ला युद्ध के आधार पर योजना बनाई और सेना को भी अपने साथ लेना चाहा, मगर जैसा हमने देखा, इनके नेता भी अनुभवी नहीं थे और अधिकतर क्रान्तिकारी विचारधारा के ही अनुयायी रहे। देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने विदेशी सरकारों से सहायता लेने में संकोच नहीं किया और ग़दर पार्टी में इस आधार पर फूट भी पड़ गई। ग़दर आंदोलन और कामागाटामारू प्रकरण का विस्तृत विवरण अलग से एक अन्य आर्टिकल में दिया गया है।
इस आंदोलन की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ये लोग देश को आजाद तो करवाना चाहते थे मगर स्वतंत्रता के पश्चात् कैसा समाज बनाना चाहिए इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये मतवाले देशभक्त थे मगर आज़ादी के बाद जनजीवन को बदलने और सामाजिक परिवर्तन लाने के बारे में वे चिंतित नहीं थे जिसके कारण वे भारत की जनता को अपने साथ नहीं ले पाए, विशेषकर उस समय जब सभी मुख्य पार्टियाँ भारत सरकार के साथ थीं। इन्हीं कारणों से इस समय के कई क्रांतिकारी, जैसे लाला हरदयाल और भाई परमानंद, हिंदू राष्ट्रवादी बने मगर ग़दर पार्टी के कई नेता, जो बाद में रूसी क्रांति से प्रभावित हुए, साम्यवादी बने और उहोंने दूसरे चरण की क्रांति और साम्यवादी आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
फिर भी इन वीरों की स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने बलिदान और मौत से जूझने का जो साहस दिखाया और जिस तरह ये देश की ख़ातिर हँसते-हँसते अपनी जान गॅवाई और फाँसी के तख्ते पर लटके उससे देश के युवकों पर बहुत प्रभाव पड़ा और आने वाले वर्षों में उन्होंने आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया।