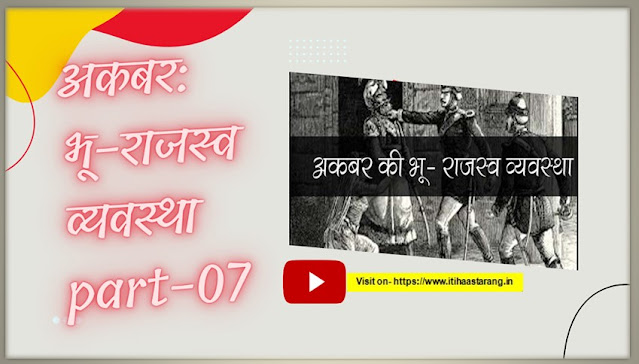Introduction (विषय-प्रवेश):
अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के राजस्व को दो भागों में बाँटा जा सकता है- केन्द्रीय अथवा शाही तथा स्थानीय अथवा प्रान्तीय। स्थानीय राजस्व स्पष्टतः बिना केन्द्रीय सरकार के वित्त-सम्बन्धी अधिकारियों से पूछे ही वसूला तथा खर्च किया जाता था। यह विभिन्न छोटे-छोटे करों से प्राप्त किया जाता था, जो उत्पादन एवं उपभोग, व्यापार एवं धंधों, सामाजिक जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा सबसे अधिक परिवहन पर लगाये जाते थे। केन्द्रीय राजस्व के प्रधान साधन थे- भूमि-राजस्व, चुंगी, टकसाल, उत्तराधिकार, लूट एवं हर्जाना, उपहार, एकाधिकार तथा प्रत्येक मनुष्य पर लगने वाला कर (पॉल-टैक्स)। जबकि स्थानीय आय चुंगी, नाव और सड़क पर तथा बहुत कुछ अन्य ’अव्वाबों’ (करों) द्वारा होती थी। उपर्युक्त साधनों से जो आय होती थी, वह भूमि द्वारा होने वाली आय का बहुत छोटा-सा भाग था। मोरलैण्ड ने भूमि द्वारा होने वाली आय का जो हिसाब लगाया है, उसके अनुसार अकबर के शासनकाल के अन्तिम वर्षों में यह आय ६ करोड़ रुपये की बैठती थी।
इनमें पुराने जमाने की तरह राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था- भू-राजस्व। कृषि योग्य भूमि तीन वर्गो में विभाजित थी – खालसा, जागीर और मदद-ए-माश। खालसा भूमि सरकारी भूमि होती थी जिससे प्राप्त आया सीधे सरकारी खजाने में जमा होती थी। जागीर भूमि राज्य के प्रमुख सरदारों या व्यक्तियों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी जिनपर उन्हे ही कर वसूल करने का अधिकार होता था तथा मदद-ए-माश भूमि को अनुदान के रुप में विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था और इस भूमि की आय पर धार्मिक व्यक्तियों का अधिकार होता था। राज्य के लिए खालसा भूमि ही राजस्व का साधन होती थी। अकबर ने शासन की बागडोर अपने हाथों में सॅभालते ही राज्य की आय के अराजकता, मुख्य स्रोत भू-राजस्व की महत्ता को समझते हुए भू-राजस्व प्रशासन में व्याप्त दस्तावेजों में गडबडी, किसानों के अनावश्यक शोषण तथा राज्य की आय में अनिश्चितता की स्थिती को सुधारने तथा अपने साम्राज्य में भू-राजस्व प्रशासन में एकरुपता लाने के प्रयास प्रारंभ कर दिये।
इस दिशा में अकबर ने कई प्रयोग कर डाले। पहला प्रयोग 1563 ई0 में एतमाद खाँ के अधीन हुआ जिसमें संपूर्ण साम्राज्य का 18 परगनों में विभाजन हुआ और प्रत्येक परगने में एक करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। 1564 ई0 में मुज्जफर खाँ के अधीन दूसरा प्रयोग किया गया जब मुज्जफर खाँ को दीवान नियुक्त किया गया और टोडरमल उसके सहायक के रुप में नियुक्त किये गये। 1568-69 ई0 में शासन के तेरहवें वर्ष शिहाबुद्दीन अहमद के अधीन तीसरा प्रयोग किया गया। इसने नस्क अथवा कनकूत प्रणाली पर बल दिया जिसके अन्तर्गत फसल की बिना नाप-तौल किये ही जमीन की पैदावार का एक सामान्य अन्दाजा लगा कर औसत कर का निर्धारण कर दिया जाता था।
चौथा प्रयोग शासनकाल के पन्द्रहवें वर्ष 1570-71 ई० में किया गया था, जबकि प्रत्येक परगने के लिए अलग-अलग भूमि-कर दरों की नयी अनुसूचियाँ भूमि की असल पैदावार के आधार पर तैयार की गयी थीं। इस कर-प्रणाली के अन्तर्गत इस बार जागीरी-भूमि भी आ गयी, जो अब तक वित्त मन्त्रालय के नियन्त्रण के बाहर ही रहती आयी थी। ’नस्क’ प्रणाली त्याग दी गयी और सरकारी अधिकारियों द्वारा जमीन की उचित नाप-जोख तथा खेतों की कुल असल पैदावार को आँकने के आधार पर कर निर्धारण के दरों की अनुसूची तैयार की गयी थी। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने व्यक्तिगत रुप से भू-राजस्व पर विशेष ध्यान दिया और 1573 ई0 में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोडकर समस्त उत्तर भारत में करोडी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जिनकी संख्या 182 थी। इनका प्रमुख कार्य राजस्व के रुप में एक करोड दाम वसूल करना था। इस प्रणाली के जन्मदाता राजा टोडरमल थे।
यह प्रणाली बहुत सफल सिद्ध हुई, क्योंकि इस आधार पर तैयार की गयी कर-अनुसूची आगामी दस वर्षों 1580 ई० तक काम में लायी जाती रही। इसके पश्चात अकबर ने और बड़ा प्रयोग किया। यह प्रयोग भूमि-कर को नकदी में प्रस्तुत करना था। यद्यपि विभिन्न प्रकार के अनाजों पर भूमि-कर की दरें दस वर्षों तक बदली नहीं थीं, तथापि इनके दाम, जिनके आधार पर वस्तुओं की जगह सरकारी मालगुजारी नकदी में बदल दी जाती थी, एक-दूसरे साल में अदलते-बदलते रहते थे और प्रत्येक वर्ष इन पर सम्राट की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती थी। इसका परिणाम यह होता था कि मालगुजारी इकट्ठी करने में विलम्ब हो जाया करता था, क्योंकि सम्राट के एक स्थान पर न रहने के कारण प्रस्तुत किये गये मालगुजारी पन्नों पर मूल्य निर्धारण के लिए शीघ्र ही आज्ञाएं जारी नहीं हो पाती थीं। इस असुविधा से बचने के विचार से कर-निर्धारण की अनुसूचियों को वस्तुओं में प्रस्तुत न करवाकर नकद रुपया आना-पाई में प्रस्तुत करवाना आरम्भ कर दिया और ये मूल्य जिनके आधार पर वस्तुएँ नकदी में बदली जाती थीं, विभिन्न स्थानों में प्रचलित पिछले दस वर्षों के मूल्यों के औसत पर निश्चित किये गये थे। यही मालगुजारी बन्दोबस्त 1580 ई० में जब्ती प्रणाली या ’आईने-दहसाला’ आज्ञापत्र के नाम से जारी किया गया। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू की गई। दक्षिण भारत में आइन-ए-दहसाला प्रणाली को शाहजहॉ के शासनकाल में मुर्शिद कुली खॉन ने लागू किया था।
आइन-ए-दहसाला :
इसके अनुसार सर्वप्रथम, साम्राज्य की सम्पूर्ण भूमि एक समान माप-प्रणाली द्वारा, जो इलाही गज, जिसकी मात्रा 41 अंगुल या 33 इंच की थी, के आधार पर नापी जाती थी। गज-माप पर आधारित ’जरीब’ जिसका इस्तेमाल शेरशाह ने किया था, सन या पटवे की रस्सी की बनायी जाती थी और गरम तथा ठण्डे मौसम में यह सिकुड़ और बढ़ भी जाती थी। इसकी जगह अकबर ने बांस की ‘जरीब‘ चालू की, जिसके टुकड़े लोहे की पत्तियों से जुड़े होते थे। बीघा जो क्षेत्रफल की इकाई था, 60 गज ग् ६० गज अथवा 3600 वर्ग गज का होता था। प्रत्येक गांव, परगना, काश्तकार के अधीन कृषि-योग्य भूमि को निश्चित किया जाता था। कृषि-योग्य सम्पूर्ण भूमि चार श्रेणियों में विभक्त की गई –
- पोलज भूमि प्रथम श्रेणी की भूमि को कहा जाता था और इस पर सदैव खेती होती थी।
- परौती भूमि भी लगभग सदैव ही खेती करने योग्य थी, लेकिन पुनः उर्वरा-शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक दो वर्ष के लिए यह खाली पड़ी रहती थी।
- छच्छर या चाचर भूमि पर तीन अथवा चार वर्ष के लिए खेती नहीं होती थी।
- बंजर भूमि पांच वर्ष अथवा और अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ दी जाती थी।
यहॉ यह उल्लेखनीय है कि भूमियों की इस श्रेणी-विभाजन का आधार भूमि की किस्म अथवा उसका उपजाऊपन नहीं था, बल्कि इस पर होने वाली काश्त का निरन्तर जारी रहना था। पुनः यदि बंजर भूमि को हम अलग कर दे तो तीन प्रकार की भूमियों को उत्पादकता के आधार पर तीन श्रेणीयों में –उत्तम, मध्यम और निम्न में बाटॉ जाता था। इस प्रकार उपर्युक्त कुल 9 प्रकार की प्रत्येक भूमि की औसत पैदावार निकाली जाती थी; जो प्रत्येक प्रकार की भूमि की स्टैण्डर्ड पैदावार समझी और मानी जाती थी और पिछले दस वर्षों की पैदावार के आधार पर प्रत्येक फसल की प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाला जाता था। सरकार औसत पैदावार का एक-तिहाई भाग भू-राजस्व के रुप में निर्धारित करती थी। सामान्यतः भू राजस्व की दर कुल उपज की 1/3 थी किंतु मोरलैण्ड और इरफान हबीब का मानना है कि भू राजस्व की दर उत्पादन का आधा या तीन चौथाई थी। कश्मीर में अकबर ने कुल उत्पादन के आधे भाग की वसूली का आदेश दिया था। आई0ए0एच0 कुरैशी का मानना है कि संभवतः भू-राजस्व एक तिहाई ही लिया जाता था। भू-राजस्व या मालगुजारी वस्तु रूप में न लेकर नकद रुपयों, आनों और पाइयों में ली जाती थी। इसके लिए अकबर ने अपने सम्पूर्ण साम्राज्य को बहुत-से दस्तूरों में विभक्त कर रखा था।
उपर्युक्त हिसाब के आधार पर ही प्रत्येक काश्तकार पर ’कर’ लगाया जाता था। काश्तकारों पर कर-निर्धारण के लिए अब तो केवल भूमि की किस्म, उसका क्षेत्रफल तथा किस मौसम में क्या-क्या काश्त हुई है, आदि बातों की जानकारी ही आवश्यक थी। इसके आधार पर सरकार और काश्तकार दोनों को ही मालगुजारी क्या लेनी-देनी है; इसका हिसाब लगाना पड़ता था। खेतों में बीज बोये जाने के एक-आध महीने के अन्दर ही सरकारी कर्मचारी इसका हिसाब तैयार कर सकते थे कि सरकार को क्या मालगुजारी लेनी है। मुगलकालीन कृषक वर्ग को तीन श्रेणीयों में बॉटा गया है –
- खुदकाश्त – वे किसान जो खुद या स्वयं की भूमि पर स्थायी और वंशानुगत कृषि करते थे।
- पाहीकाश्त – वे किसान जो दूसरे गॉवों में जाकर अस्थायी रुप से बटाईदार के रुप में कार्य करते थे।
- मुजारियान – वे किसान जो खुदाकाश्त प्रकार के कृषक की जमीन को किराये पर लेकर उसपर खेती करते थे।
’आइन-ए-दहसाला’ के सम्बन्ध में इतिहास के विद्वानों में मतभेद है। वी०ए० स्मिथ ने इसे दस साल का बन्दोबस्त माना है और उनका मत है कि यह पिछले दस वर्षों की औसत पैदावार पर आधारित है। दूसरी ओर मोरलैण्ड ने, जिन्होंने मुगलकालीन भू-राजस्व सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने में अपने बीस वर्ष लगाये थे, केवल दस साल के नकद करों की मांग के औसत का हवाला दिया है और प्रत्येक फसल में प्रत्येक प्रकार की भूमि की दस वर्ष की औसत पैदावार का कोई जिक्र नहीं किया। वास्तव में इस विषय का सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि 1580 ई० का अकबर का यह बन्दोबस्त पिछले दस वर्षों की औसत पैदावार पर आधारित था और पिछले दस वर्षों के औसत मूल्यों पर वस्तुरूपी सरकारी लगान रुपयों में बदला जाता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, औसत पैदावार निश्चित करने के लिए प्रत्येक परगना एक इकाई माना जाता था और मूल्य निश्चित करने के लिए ’दस्तूर’ को इकाई माना जाता था। यह निश्चित कहा जाता है कि यह बन्दोबस्त स्थायी नहीं था और न यह वार्षिक ही था।
यह प्रणाली खालसा भूमि-क्षेत्रों में ही लागू की गयी थी लेकिन 1581-82 में इसके अन्तर्गत जागीरी भूमि भी आ गयी। अब जागीरदार मनचाहे ढंग से ’जागीरों’ की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। साथ ही बंजर भूमि को भी उर्वरा भूमि में परिवर्तित करने की यथासंभव चेष्टा की गयी। इसके लिए सरकार उन काश्तकारों को ऋण देती थी जो बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए परिश्रम करते थे। बन्दोबस्त सीधा काश्तकारों से ही किया जाता था इसलिए इस प्रणाली को भी रैयतवाडी पद्धति कहा जाता है। प्रत्येक काश्तकार को एक ’पट्टा’ दिया जाता था और कबूलियत (शर्तनामा) पर उसके हस्ताक्षर कराये जाते थे। इन कागजातों में काश्तकार के अधीन भूमि का ब्यौरा, भूमि का क्षेत्रफल तथा लगान, जो उसे देना है, दर्ज रहता था। यदि किसी गांव अथवा परगने में अनावृष्टि अथवा अन्य किसी प्रकार की दैविक आपत्ति द्वारा फसलें चौपट हो जाती थीं तो सरकार की ओर से माफी प्रदान की जाती थी। मालगुजारी एकत्र करने का काम परगनों और जिलों में सरकारी अधिकारियों, आमिल तथा अमलगुजार के सुपुर्द था। इस कार्य में इन्हें कानूनगो, गांव के पटवारी और मुखिया की भी सहायता मिलती रहती थी। भूमि-सर्वे से सम्बन्धित अमीन, शिकदार, अपील, बितिक्ची तथा दूसरे अन्य कर्मचारियों के निर्देशन के लिए पैदावार आंकने और मालगुजारी इकट्ठी करने के सम्बन्ध में प्रत्येक परगने में ’दस्तूरुल अमल’ तथा शिक्षाप्रद आदेश लिखित रूप में प्रस्तुत किये जाते थे। इतिहासकार स्मिथ ने इस प्रणाली की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।
अकबर के शासनकाल में इस प्रथा के अनुसार ठीक-ठाक काम होता रहा किन्तु जहॉगीर के शासनकालमें इस प्रथा में दोष आने लगे। शाहजहॉ और औरंगजेब के समय में सरकार ने अकबर के रैयतवाडी बन्दोबस्त के साथ ठेकेदारों को भी भूमि कर वसूली को देना प्रारंभ कर दिया जो अत्यन्त हानिकारक साबित हुआ। पहले तो जागीरी भूमि में रैयतवाडी पद्धति को बन्द किया गया और फिर खालसा भूमि में ठेकेदारी प्रथा जारी कर दी गयी। इस प्रकार अकबर के पश्चात मुगल शासकों के समय में टोडरमल का बन्दोबस्त बिल्कुल समाप्त हो गया और ठेकेदारी प्रथा जारी हो गयी।
अकबर का व्यक्तित्व और विश्लेषण–
सम्राट अकबर निःसन्देह समस्त मुस्लिम शासकों में एक महान् शासक माना जाता है। उसका व्यक्तित्व और कृतित्व उसे भारत ही नहीं विश्व के महान् शासकों की प्रथम पंक्ति में खड़ा करते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व और प्रखर मस्तिष्क का धनी अकबर अदम्य साहस, असाधारण प्रतिभा और अनेक शासकोचित गुणों से विभूषित था। गैरेट के अनुसार अकबर एक साहसी सैनिक, महान् सेनानायक तथा बुद्धिमान शासक था। उसकी गणना इतिहास के महानतम सम्राटों में की जा सकती है। स्मिथ महोदय के अनुसार, अकबर जन्मजात सम्राट् था और इतिहास जितने भी सम्राटों को मानता है, उनमें महान् पद पर बैठने का उसका दावा सर्वथा उचित था। उसका यह दावा उसके प्राकृतिक गुणों पर आधारित तथा उसके द्वारा सुरक्षित था। उसके मौलिक विचार और उसकी उपलब्धियाँ उसकी नींव को मजबूत करती थीं।
इन उज्जवल पक्षों के साथ ही साथ अकबर के जीवन से जुडे कुछ काले पक्ष भी है जिसको लेकर समय समय पर इतिहासकारों द्वारा अकबर की आलोचना की जाती रही है। कुछ आलोचकों का मानना है कि अकबर का व्यक्तित्व उतना पूर्ण और मर्यादित नही था जितना अबुल फजल ने चित्रित किया है। इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं, कि हम अकबर को उसके दरबार के इतिहास और वर्णनों जैसे अकबरनामा आदि के अनुसार महान कहते हैं। यदि कोई अन्य उल्लेखनीय कार्यों की ओर देखे, जैसे दलपत विलास, तब स्पष्ट हो जाएगा कि अकबर अपने हिन्दू सामंतों से कितना अभद्र व्यवहार किया करता था। अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह द्वारा विश्वनाथ मंदिर के निर्माण को अकबर की अनुमति के बाद किए जाने के कारण हिन्दुओं ने उस मंदिर में जाने का बहिष्कार कर दिया। कारण साफ था, कि राजा मानसिंह के परिवार के अकबर से वैवाहिक संबंध थे। अकबर के हिन्दू सामंत उसकी अनुमति के बगैर मंदिर निर्माण तक नहीं करा सकते थे। बंगाल में राजा मानसिंह ने एक मंदिर का निर्माण बिना अनुमति के आरंभ किया, तो अकबर ने पता चलने पर उसे रुकवा दिया और 1595 ई0 में उसे मस्जिद में बदलने के आदेश दिए।
अकबर के लिए आक्रोश की हद एक घटना से पता चलती है। हिन्दू किसानों के एक नेता राजाराम ने अकबर के मकबर, सिकंदरा को लूटने का प्रयास किया, जिसे स्थानीय फ़ौजदार मीर अबुल फजल ने असफल कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद 1688 में राजा राम सिकंदरा में दोबारा प्रकट हुआ और शाइस्ता खां के आने में विलंब का फायदा उठाते हुए उसने मकबरे पर दोबारा सेंध लगाई और बहुत से बहुमूल्य सामान जैसे सोने, चाँदी, बहुमूल्य कालीन, चिराग, इत्यादि लूट लिए तथा जो ले जा नहीं सका, उन्हें बर्बाद कर गया। राजा राम और उसके आदमियों ने अकबर की अस्थियों को खोद कर निकाल लिया एवं जला कर भस्म कर दिया, जो कि मुस्लिमों के लिए घोर अपमान का विषय था। तत्कालीन समाज में वेश्यावृति को सम्राट का संरक्षण प्रदान था। अकबर अपनी प्रजा को बाध्य किया करता था की वह अपने घर की स्त्रियों का नग्न प्रदर्शन सामूहिक रूप से आयोजित करे जिसे अकबर ने खुदारोज (प्रमोद दिवस) नाम दिया हुआ था। इस उत्सव के पीछे अकबर का एकमात्र उदेश्य सुन्दरियों को अपने हरम के लिए चुनना था। प्रति सप्ताह आगरे के किले के सामने मैदान में लगाये जाने वाले मीना बाजार में अकबर द्वारा सुन्दर रमणियों की तलाश की कथाएॅ बहुत प्रचलित है। इस मीना बाजार से सुन्दर लडकियॉ तलाश कर अकबर के हरम में रखी जाती थी। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर की पत्नी से सम्बन्धित कथाएॅ भी बहुत प्रचलित है जिसमें उसने अपने सतीत्व और मान-मर्यादा की रक्षा के लिए कटार निकाली थी। वह मादक पदार्थो का भी प्रयोग करता था और छल कपट का भी व्यवहार करता था। इस प्रकार के अनेक उदाहरण पेश कर आलोचकों ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि अकबर का व्यक्तित्व पूर्णत मर्यादित नही था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त आरोप निराधार है और सिर्फ आलोचना के कारण उपरोक्त बाते कही गयी है। सामान्य परिस्थितीयों में हम यह नही कह सकते कि मानसिक दुर्बलताओं के आवेग में उसने कोई असंयमी कार्य किया होगा।
निस्सन्देह अकबर एक महान् विजेता, विशाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, साहसी सेनानायक, सुयोग्य शासक तथा प्रजावत्सल सम्राट् था। वैसे तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय सम्राट् बाबर को दिया जाता है किन्तु मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर एक विशाल, सुगठित तथा सुव्यवस्थित साम्राज्य के स्थायी आधारों के निर्माण का श्रेय अकबर को ही है। एक शासक के रूप में सम्राट् अकबर की सफलता का सबसे बड़ा आधार यह था कि उसने विभिन्न राज्यों, विभिन्न जातियों तथा विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों को एक सूत्र में बाँधने का सराहनीय कार्य किया। उसका विशाल साम्राज्य 15 सूबों में बंटा हुआ था और उसने प्रत्येक सूबे को सबल और सफल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की, ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रशासनिक एकरूपता और कार्यपरक सक्षमता का समन्वय था। जब 1556 ई0 में वह सिंहासन पर बैठा, तब भारत छोटे-छोटे अनेक हिन्दू-मुस्लिम राज्यों में विभक्त था जो परस्पर एक-दूसरे को आत्मसात करने या नतमस्तक करने के लिए कटिबद्ध थे किन्तु 1605 ई. में जब उसका देहान्त हुआ, तब वह साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारतवर्ष के विशाल भू-भाग पर छाया हुआ था। अकबर के कुशल शासन के कारण उस युग में भारत ने प्रगति और उन्नति के अनेक कीर्तिमान आयाम स्थापित किये थे। अकबर-युग में भारत ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की, प्रत्युत साहित्य और कला की दृष्टि से भी अभूतपूर्व प्रगति की थी। उसके दरबार में 9 महत्वपूर्ण विद्वतजन निवास करते थे जिसे अकबर के ‘नवरत्न के नाम से जाना जाता है। इनमें अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुर्रहीम खानखाना, फकीर अजीओं-दिन और मुल्ला दो पियाजा शामिल थे। यद्यपि अकबर स्वतः औपचारिक शिक्षण का पूरा लाभ नहीं उठा सका था किन्तु बहुश्रुत था तथा विद्वानों और कलाकारों का उदार संरक्षक था। डॉ0 आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव ने अकबर का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, अकबर का युग महान सम्राटों का युग था, अकबर के समकालीन महान् शासकों में इंग्लैण्ड की एलिज़ाबेथ, फ्रांस को हेनरी चतुर्थ तथा पर्शिया के अब्बास महान् था किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि अकबर इन सबसे एक नहीं अनेक दृष्टियों से श्रेष्ठ था।”
Tags
मध्यकालीन भारत